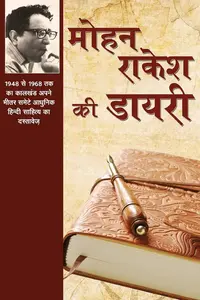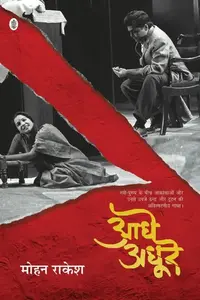|
नाटक-एकाँकी >> लहरों के राजहंस (सजिल्द) लहरों के राजहंस (सजिल्द)मोहन राकेश
|
96 पाठक हैं |
||||||
सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध...
Laharon ke raj hans
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उनके बीच खड़े हुए व्यक्ति के द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वन्द्व निहित है। इस द्वन्द्व का एक दूसरा पक्ष स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध है। जीवन के प्रेय और श्रेय के बीच एक कृत्रिम और आरोपित द्वन्द्व है, जिसके कारण व्यक्ति के लिए चुनाव कठिन हो जाता है और उसे चुनाव करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाती। चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा-बीज और उसका केन्द्र-बिन्दु है। धर्म-भावना से प्रेरित इस कथानक में उलझे हुए ऐसे ही अनेक प्रश्नों का इस कृति में नए भाव-बोध के परिवेश में परीक्षण किया गया है। सुंदरी के रूपपाश में बँधे हुए अनिश्चित, अस्थिर और संशयी मन वाले नंद की यही स्थिति होनी थी कि नाटक का अंत होते-होते उसके हाथों में भिक्षापात्र होता और धर्म-दीक्षा में उसके केश काट दिये जाते।
लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन के भावबोध का जो संवेदन दिया गया है, वह इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रेष्ठ और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है, जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा-स्थितियों को ‘अनैतिहासिक’ और ‘युगीन’ बना दे तथा कथा के अंतर्द्वन्द्व को आधुनिक अर्थ-व्यंजना प्रदान कर दे।
सभी देशों के नाटक-साहित्य के इतिहास में विभिन्न युगों में जब भी श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई है, तब नाटककारों ने प्राचीन कथानकों को नई दृष्टि से देखा है और उनको नई अर्थ-व्यंजना दी है। उसी परम्परा में मोहन राकेश का यह नाटक भी है जो अध्ययन-कक्षों तथा रंगशालाओं में पाठकों और दर्शकों, दोनों को रस देता है।
लहरों के राजहंस के कथानक को आधुनिक जीवन के भावबोध का जो संवेदन दिया गया है, वह इस ऐतिहासिक कथानक को रचनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। वास्तव में ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर श्रेष्ठ और सशक्त नाटकों की रचना तभी हो सकती है, जब नाटककार ऐतिहासिक पात्रों और कथा-स्थितियों को ‘अनैतिहासिक’ और ‘युगीन’ बना दे तथा कथा के अंतर्द्वन्द्व को आधुनिक अर्थ-व्यंजना प्रदान कर दे।
सभी देशों के नाटक-साहित्य के इतिहास में विभिन्न युगों में जब भी श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटकों की रचना हुई है, तब नाटककारों ने प्राचीन कथानकों को नई दृष्टि से देखा है और उनको नई अर्थ-व्यंजना दी है। उसी परम्परा में मोहन राकेश का यह नाटक भी है जो अध्ययन-कक्षों तथा रंगशालाओं में पाठकों और दर्शकों, दोनों को रस देता है।
देर आयद दुरुस्त आयद
कम लोग जानते हैं कि 1968 में लहरों के राजहंस का एक संशोधित परिवर्तित नया रूप प्रकाशित हुआ था। उसकी भूमिका के अन्त में राकेश ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इस नाटक के 1963 में छपे प्रथम रूप का प्रकाशन भविष्य में नहीं होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से पता नहीं किन ज्ञात अज्ञात कारणों के चलते, तब से अब तक इस नाटक का पहला रूप ही लगातार छपता और बिकता रहा है। उसी के गुण दोषों को बार-बार दोहराते बहुसंख्यक शोध एवं आलोचना ग्रन्थ इस बीच लगातार लिखे और पढ़े पढ़ाए जाते हैं। यह सच है कि कुछ नाटक समीक्षकों एवं रंगकर्मियों को आज भी इस नाटक का पहला रूप नए के मुकाबले बेहतर प्रतीत होता है और कुछ नाट्य निर्देशकों ने इस बीच दोनो विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद अभिमंचन के लिए प्रथम संस्करण वाले आलेख को ही चुना भी है। परन्तु मेरे विचार से इस विवादास्पद प्रश्न पर लेखकीय इच्छा का ही सम्मान होना चाहिए-क्योंकि राकेश ने तो नए के साथ-साथ पुराने रूप के भी छपते रहने के सुझाव का भी स्पष्ट विरोध किया था। हमें विश्वास है कि लेखकीय सम्मान और गरिमा के प्रतीक बन चुके रचनाकार मोहन राकेश के जीवित रहते उसकी इच्छा का ऐसा अनादर कभी सम्भव नहीं होता।
लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। अब लहरों के राजहंस के नए रूप के पुनर्प्रकाशन के साथ पैंतीस वर्ष बाद ही सही राकेश की उस अन्तिम इच्छा पूर्ति हो रही है तो हम सबके लिए निश्चय ही यह सन्तोष और प्रसन्नता की बात है। प्रकाशक का यह आश्वासन और भी सुखकर है कि नाटककार की इच्छानुसार इस नाटक के पुराने रूप का प्रकाशन भविष्य में नहीं किया जाएगा। अब पाठकों को केवल इसका यह नया रूप ही उपलब्ध होगा। हमें विश्वास है कि इससे आलोचकों शिक्षाओं और रंगकर्मियों के बीच इस नाटक के प्रति नई उत्सुकता जागेगी और इसके समुचित मूल्यांकन से रचना और रचनाकार को न्याय मिल सकेगा।
सन् छियालीस सैंतालीस में सुन्दरी नन्द, अलका और मैत्रेय को लेकर लिखी गई एक ‘अनाम ऐतिहासिक कहानी’ से लेकर सन् छियासठ-सड़सठ में लिखे रंग नाटक लहरों के राजहंस के नए रूप में लिखे जाने की बीस बाईस वर्ष लम्बी, जटिल और रचनात्मक अन्तर्यात्रा की अन्तरंग कथा तो इसी संस्करण के साथ प्रकाशित आलेख नाटक का यह परिवर्तित रूप में स्वयं नाटककार ने ही लिख दी है। अतः यहाँ इस नाटक के पुराने और नए रूप की भिन्नता के कुछ सूक्ष्म एवं महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करना इसे सही सन्दर्भ एवं परिप्रेक्ष्य देने की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होता है।
लहरों के राजहंस के दोनों रूपों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पहले संस्करण में नाटक का परदा पर श्वेतांग का श्यामांग के प्रति संवाद था-‘(कार्य में व्यस्त) तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई ?’ परन्तु नए रूप में परदा उठने पर अँधेरे में नेपथ्य से त्रिशरणो के समवेत-स्वर की प्रभावपूर्ण योजना की गई है। इससे मूल नाटक के आरम्भ होने से पहले ही दर्शक-पाठक का मन ‘बौद्धकाल’ में चला जाता है और सुन्दरी के विरुद्ध गौतम बुद्ध की अप्रत्यक्ष परन्तु प्रभावी शक्ति का पूर्व संकेत भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त श्वेतांग के एक पंक्ति के संवाद को अब तीस पंक्तियों के लम्बे संवाद में बदल दिया गया है जो ‘क्या बात है, नागदास’ से आरम्भ होकर तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई ? तक चलता है। इससे कामोत्सव की चहल-पहल, हलचल तैयारी महत्त्व और राजसी समारोहपूर्ण वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है।
नए रूप में श्यामांग के प्रतीकत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। इस दृष्टि से कुछेक नए संवाद भी जोड़े गए हैं, जैसे-
सुन्दरी : (अधीर भाव से झूले से उठती हुई)
‘जिससे आपको विशेष अनुराग है। जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है। जिसकी बातों में आपको अपने अन्तर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है। जानती हूँ।’
नए संस्करण में पहले अंक का अन्त एक अत्यन्त तनावपूर्ण स्थिति में मैत्रेय के प्रस्थान और नन्द के आत्मोन्मुख संक्षिप्त और सारगर्भित संवाद से होता है। पहले संस्करण के अन्त में मैत्रेय के प्रस्थान के बाद शशांक का प्रवेश और नन्द का यह आदेश भी था, "तुमसे कह दिया है जाओ। जो आसन बिछाए हैं, उठा दो। अब उन सबकी कोई आवश्यकता नहीं है।’ नन्द का यह संवाद अन्त की तीव्रता कम कर देता है और नन्द के अन्तर्मुखी चरित्र को एक चतुर, व्यावहारिक व्यक्ति का रूप दे देता है, जो उसके समग्र व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। नए अन्त में एक कुतूहल, पैनापन और क्षिप्रता है। नन्द का अन्तिम संवाद अब दूसरे अंक में नन्द की भूमिका को ठोस धरातल प्रदान करता है।
दूसरे अंक के आरम्भ में ‘संगीत खंडों के समान’ नेपथ्य से आने वाले श्यामांग के लम्बे प्रलापपूर्ण संवादों को संक्षिप्त कर दिया गया है और सुन्दरी के जागने से पहले नन्द के एक लम्बे एकालाप की योजना की गई है। यह एकालाप नन्द के व्यक्तित्व को गहराई से प्रतिष्ठित करता है और उसके चरित्र की अनेक परतें उघाड़ता हुआ उसके जटिल अन्तर्द्वन्द्व की झलक भी पाठक दर्शक को दे देता है। पहले अंक के अन्त और दूसरे अंक के आरम्भ के बीच के अन्तराल को भी यह एकालाप भरने का प्रयास करता है। दर्पण अब कांच के स्थान पर कच्चे रजत का हो गया है जो देश काल के अनुरूप है।
पहले संस्करण में दूसरे अंक का अन्त नेपथ्य से श्यामांग के ‘पानी...पानी नहीं है, से लेकर ‘कोई एक किरण...’ वाले प्रलाप से होता था परन्तु नए रूप में यह मन्त्र मुग्ध नन्द के प्रस्थान और सुन्दरी के विडम्बनापूर्ण संक्षिप्त संवाद से होता है-यह अपेक्षाकृत तेज कसावपूर्ण और नाटकीय अन्त है।
तीसरे अंक का आरम्भ दोनों संस्करणों में पूर्णतः समान है।
नन्द के केश-कर्तन की सूचना का प्रसंग, नए संस्करण में अलका और श्वेतांग के बीच और बढ़ा दिया गया है। इससे नन्द के अन्तर्द्वन्द्वपूर्ण क्षणों की विस्ततृ सूचना तो मिलती है, परन्तु नाटक की संरचना शिथिल हो जाती है और पाठक-दर्शक की रुचि भी इस प्रसंग में काफी क्षीण हो जाती है।
नए संस्करण में भिक्षु आनन्द और नन्द के वार्तालाप का भी विस्तार किया गया है। इसमें नन्द के दीक्षा- प्रसंग और बाघ-युद्ध की दुबारा सूचना मिलती है-जो दर्शक पाठक को उबा देती है।
तीसरे अंक का अन्तिम अंश नए संस्करण में बिलकुल बदल दिया गया है। पहले रूप में सुन्दरी के जागने पर नन्द मंच से हट जाता है। नन्द और सुन्दरी अलका तथा श्वेतांग के माध्यम से एक-दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुन्दरी से मिले बिना ही नन्द एक लम्बा-सा एकालाप बोलकर ‘अपने केशों की खोज’ में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। सुन्दरी नन्द द्वारा अपने को गलत या न समझे जाने की बात कहती है और नेपथ्य से श्यामांग के प्रलापपूर्ण लम्बे संवाद से नाटक समाप्त हो जाता है। परन्तु नए संस्करण में राकेश ने नन्द और सुन्दरी को एक-दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। वे एक-दूसरे से मिलते हैं, टकराते हैं और एक भीषण विस्फोट के साथ (जिसमें औपचारिकता के आवरण तार-तार हो गए हैं) एक-दूसरे से छिटककर अलग हो जाते हैं।
नए संस्करण में तीसरे अंक का उत्तरार्द्ध अपनी वैचारिकता, गम्भीरकता, तीव्रता और नाटकीयता की दृष्टि से हिन्दी नाट्य साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धि है। नन्द और सुन्दरी के तनावपूर्ण नुकीले संवादों से नाटक संतूर के तारों की तरह लगातार कसता चला जाता है और चरम पर पहुँच कर जैसे एक झटके से सम्बन्ध का तार झनझनाकर टूट जाता है। कहीं जरा-सा भी ढीलापन नहीं है यहाँ; साँस लेने तक का अवकाश नहीं है।
‘....जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था, उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बना कर फेंक दिया गया है....।’ तथा अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच में चेतना को एक प्रश्नचिह्न बनाकर छोड़ दिया गया है...। जैसे बहुउद्धृत सैद्धान्तिक संवादों को भी नए संस्करण में स्थान नहीं दिया गया। ‘मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ’ वाला संवाद भी स्वागत- कथन के रूप में था, अब उसे सुन्दरी से सीधे वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नए संस्करण में वैसे अनेक और अधिकांश स्थानों पर संवादों को माँजा-सँवारा गया है परन्तु सुन्दरी के संवादों में विशेष रूप से एक नई चमक पैदा की गई है। अब सुन्दरी अपने आभिजात्य और अपनी गरिमा से उद्भूत संवाद लय को कहीं नष्ट नहीं होने देती।
शिल्प की दृष्टि से नए संस्करण के तीनों अंकों के अपने-अपने आरम्भ, संघर्ष और चरम बिन्दु हैं परन्तु अत्यन्त कलात्मक और नाटकीय ढंग से उन्हें एक अन्विति प्रदान की गई है।
इस प्रकार लहरों के राजहंस के इस नए संस्करण में-
इस नाटक ने नाटककार, निर्देशक और नाट्यदल के बहुप्रशंसित रचनात्मक सहयोगी-प्रयोग की शक्ति के साथ-साथ इस प्रक्रिया की सीमाओं को भी तीव्रता से उजागर किया है।
वस्तु को अधिक नाटकीय ढंग से संयोजित किया गया है।
चरित्रों की रेखाएँ अधिक स्पष्ट और प्रखर कर दी गई हैं तथा विडम्बना गहन हुई है।
लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। अब लहरों के राजहंस के नए रूप के पुनर्प्रकाशन के साथ पैंतीस वर्ष बाद ही सही राकेश की उस अन्तिम इच्छा पूर्ति हो रही है तो हम सबके लिए निश्चय ही यह सन्तोष और प्रसन्नता की बात है। प्रकाशक का यह आश्वासन और भी सुखकर है कि नाटककार की इच्छानुसार इस नाटक के पुराने रूप का प्रकाशन भविष्य में नहीं किया जाएगा। अब पाठकों को केवल इसका यह नया रूप ही उपलब्ध होगा। हमें विश्वास है कि इससे आलोचकों शिक्षाओं और रंगकर्मियों के बीच इस नाटक के प्रति नई उत्सुकता जागेगी और इसके समुचित मूल्यांकन से रचना और रचनाकार को न्याय मिल सकेगा।
सन् छियालीस सैंतालीस में सुन्दरी नन्द, अलका और मैत्रेय को लेकर लिखी गई एक ‘अनाम ऐतिहासिक कहानी’ से लेकर सन् छियासठ-सड़सठ में लिखे रंग नाटक लहरों के राजहंस के नए रूप में लिखे जाने की बीस बाईस वर्ष लम्बी, जटिल और रचनात्मक अन्तर्यात्रा की अन्तरंग कथा तो इसी संस्करण के साथ प्रकाशित आलेख नाटक का यह परिवर्तित रूप में स्वयं नाटककार ने ही लिख दी है। अतः यहाँ इस नाटक के पुराने और नए रूप की भिन्नता के कुछ सूक्ष्म एवं महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करना इसे सही सन्दर्भ एवं परिप्रेक्ष्य देने की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होता है।
लहरों के राजहंस के दोनों रूपों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पहले संस्करण में नाटक का परदा पर श्वेतांग का श्यामांग के प्रति संवाद था-‘(कार्य में व्यस्त) तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई ?’ परन्तु नए रूप में परदा उठने पर अँधेरे में नेपथ्य से त्रिशरणो के समवेत-स्वर की प्रभावपूर्ण योजना की गई है। इससे मूल नाटक के आरम्भ होने से पहले ही दर्शक-पाठक का मन ‘बौद्धकाल’ में चला जाता है और सुन्दरी के विरुद्ध गौतम बुद्ध की अप्रत्यक्ष परन्तु प्रभावी शक्ति का पूर्व संकेत भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त श्वेतांग के एक पंक्ति के संवाद को अब तीस पंक्तियों के लम्बे संवाद में बदल दिया गया है जो ‘क्या बात है, नागदास’ से आरम्भ होकर तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई ? तक चलता है। इससे कामोत्सव की चहल-पहल, हलचल तैयारी महत्त्व और राजसी समारोहपूर्ण वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है।
नए रूप में श्यामांग के प्रतीकत्व को अधिक स्पष्ट कर दिया गया है। इस दृष्टि से कुछेक नए संवाद भी जोड़े गए हैं, जैसे-
सुन्दरी : (अधीर भाव से झूले से उठती हुई)
‘जिससे आपको विशेष अनुराग है। जिससे बात करके आपको विशेष सुख मिलता है। जिसकी बातों में आपको अपने अन्तर्मन की छाया झलकती दिखाई देती है। जानती हूँ।’
नए संस्करण में पहले अंक का अन्त एक अत्यन्त तनावपूर्ण स्थिति में मैत्रेय के प्रस्थान और नन्द के आत्मोन्मुख संक्षिप्त और सारगर्भित संवाद से होता है। पहले संस्करण के अन्त में मैत्रेय के प्रस्थान के बाद शशांक का प्रवेश और नन्द का यह आदेश भी था, "तुमसे कह दिया है जाओ। जो आसन बिछाए हैं, उठा दो। अब उन सबकी कोई आवश्यकता नहीं है।’ नन्द का यह संवाद अन्त की तीव्रता कम कर देता है और नन्द के अन्तर्मुखी चरित्र को एक चतुर, व्यावहारिक व्यक्ति का रूप दे देता है, जो उसके समग्र व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। नए अन्त में एक कुतूहल, पैनापन और क्षिप्रता है। नन्द का अन्तिम संवाद अब दूसरे अंक में नन्द की भूमिका को ठोस धरातल प्रदान करता है।
दूसरे अंक के आरम्भ में ‘संगीत खंडों के समान’ नेपथ्य से आने वाले श्यामांग के लम्बे प्रलापपूर्ण संवादों को संक्षिप्त कर दिया गया है और सुन्दरी के जागने से पहले नन्द के एक लम्बे एकालाप की योजना की गई है। यह एकालाप नन्द के व्यक्तित्व को गहराई से प्रतिष्ठित करता है और उसके चरित्र की अनेक परतें उघाड़ता हुआ उसके जटिल अन्तर्द्वन्द्व की झलक भी पाठक दर्शक को दे देता है। पहले अंक के अन्त और दूसरे अंक के आरम्भ के बीच के अन्तराल को भी यह एकालाप भरने का प्रयास करता है। दर्पण अब कांच के स्थान पर कच्चे रजत का हो गया है जो देश काल के अनुरूप है।
पहले संस्करण में दूसरे अंक का अन्त नेपथ्य से श्यामांग के ‘पानी...पानी नहीं है, से लेकर ‘कोई एक किरण...’ वाले प्रलाप से होता था परन्तु नए रूप में यह मन्त्र मुग्ध नन्द के प्रस्थान और सुन्दरी के विडम्बनापूर्ण संक्षिप्त संवाद से होता है-यह अपेक्षाकृत तेज कसावपूर्ण और नाटकीय अन्त है।
तीसरे अंक का आरम्भ दोनों संस्करणों में पूर्णतः समान है।
नन्द के केश-कर्तन की सूचना का प्रसंग, नए संस्करण में अलका और श्वेतांग के बीच और बढ़ा दिया गया है। इससे नन्द के अन्तर्द्वन्द्वपूर्ण क्षणों की विस्ततृ सूचना तो मिलती है, परन्तु नाटक की संरचना शिथिल हो जाती है और पाठक-दर्शक की रुचि भी इस प्रसंग में काफी क्षीण हो जाती है।
नए संस्करण में भिक्षु आनन्द और नन्द के वार्तालाप का भी विस्तार किया गया है। इसमें नन्द के दीक्षा- प्रसंग और बाघ-युद्ध की दुबारा सूचना मिलती है-जो दर्शक पाठक को उबा देती है।
तीसरे अंक का अन्तिम अंश नए संस्करण में बिलकुल बदल दिया गया है। पहले रूप में सुन्दरी के जागने पर नन्द मंच से हट जाता है। नन्द और सुन्दरी अलका तथा श्वेतांग के माध्यम से एक-दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सुन्दरी से मिले बिना ही नन्द एक लम्बा-सा एकालाप बोलकर ‘अपने केशों की खोज’ में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। सुन्दरी नन्द द्वारा अपने को गलत या न समझे जाने की बात कहती है और नेपथ्य से श्यामांग के प्रलापपूर्ण लम्बे संवाद से नाटक समाप्त हो जाता है। परन्तु नए संस्करण में राकेश ने नन्द और सुन्दरी को एक-दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। वे एक-दूसरे से मिलते हैं, टकराते हैं और एक भीषण विस्फोट के साथ (जिसमें औपचारिकता के आवरण तार-तार हो गए हैं) एक-दूसरे से छिटककर अलग हो जाते हैं।
नए संस्करण में तीसरे अंक का उत्तरार्द्ध अपनी वैचारिकता, गम्भीरकता, तीव्रता और नाटकीयता की दृष्टि से हिन्दी नाट्य साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धि है। नन्द और सुन्दरी के तनावपूर्ण नुकीले संवादों से नाटक संतूर के तारों की तरह लगातार कसता चला जाता है और चरम पर पहुँच कर जैसे एक झटके से सम्बन्ध का तार झनझनाकर टूट जाता है। कहीं जरा-सा भी ढीलापन नहीं है यहाँ; साँस लेने तक का अवकाश नहीं है।
‘....जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था, उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बना कर फेंक दिया गया है....।’ तथा अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच में चेतना को एक प्रश्नचिह्न बनाकर छोड़ दिया गया है...। जैसे बहुउद्धृत सैद्धान्तिक संवादों को भी नए संस्करण में स्थान नहीं दिया गया। ‘मैं चौराहे पर खड़ा एक नंगा व्यक्ति हूँ’ वाला संवाद भी स्वागत- कथन के रूप में था, अब उसे सुन्दरी से सीधे वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नए संस्करण में वैसे अनेक और अधिकांश स्थानों पर संवादों को माँजा-सँवारा गया है परन्तु सुन्दरी के संवादों में विशेष रूप से एक नई चमक पैदा की गई है। अब सुन्दरी अपने आभिजात्य और अपनी गरिमा से उद्भूत संवाद लय को कहीं नष्ट नहीं होने देती।
शिल्प की दृष्टि से नए संस्करण के तीनों अंकों के अपने-अपने आरम्भ, संघर्ष और चरम बिन्दु हैं परन्तु अत्यन्त कलात्मक और नाटकीय ढंग से उन्हें एक अन्विति प्रदान की गई है।
इस प्रकार लहरों के राजहंस के इस नए संस्करण में-
इस नाटक ने नाटककार, निर्देशक और नाट्यदल के बहुप्रशंसित रचनात्मक सहयोगी-प्रयोग की शक्ति के साथ-साथ इस प्रक्रिया की सीमाओं को भी तीव्रता से उजागर किया है।
वस्तु को अधिक नाटकीय ढंग से संयोजित किया गया है।
चरित्रों की रेखाएँ अधिक स्पष्ट और प्रखर कर दी गई हैं तथा विडम्बना गहन हुई है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book